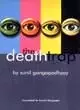|
विविध उपन्यास >> रानू और भानु रानू और भानुसुनील गंगोपाध्याय
|
297 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है एक अतुलनीय उपन्यास.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रवीन्द्रनाथ को प्रतिदिन पूरे भारत से सैकड़ों चिट्ठियाँ मिलती थीं। ये
यथासम्भव उनका जवाब भी देते थे। एक दिन पत्र पाकर कवि को बड़ा कौतुक महसूस
हुआ। उस पत्र को वाराणसी की रानू नामक एक बालिका ने लिखा था। इसी उम्र में
वह कवि का काफी साहित्य पढ़ चुकी थी। वे ही उसके सबसे करीबी व्यक्ति हो
गये थे। उसकी शिकायत थी कि कवि इन दिनों इतनी कम कहानियाँ क्यों लिख रहा
हैं। कवि ने उस बालिका के पत्र का जवाब दे दिया।
अपने ग्रहस्थ जीवन ने रवीन्द्रनाथ को कभी मानसिक सुख-शान्ति नहीं मिली थी। अचानक एक दिन लम्बी बीमारी भोगने के बाद कवि की प्रिय बेटी माधुरी लता का देहावसान हो गया। कवि टूट गये। उसी दिन अशान्त चित्त से एक भाड़े की गाड़ी लेकर वे भवानीपुर पहुँचे। नम्बर ढूँढ़ने एक घर के सामने रुककर उन्होंने पुकारा-रानू ! रानू !
अपना नाम सुनते ही तेजी से एक बालिका उतर आयी। कवि अपलक उसे देखते रह गये। यह वे किसे देख रहे थे ? यह परी थी या स्वर्ग की कोई अप्सरा ! उसी दिन अट्ठावन वर्षीय कवि से उस बालिका से विचित्र रिश्ता कायम हो गया। रानू कवि के खेल की संगिनी बन गई। नई रचनाओं की प्रेरणादात्री, उनकी खोई ‘बउठान’
और रानू के लिए कवि हो गये उसके प्रिय भानू दादा !
कवि के चीन-भ्रमण के समय उनकी अनुपस्थिति में रानू की शादी तय हो गई। रानू अब सर राजेन मुखर्जी के पुत्र वीरेन की पत्नी बन गई। दो सन्तानों की माँ।
कवि अब वृद्ध थे। उन्हें जीवन के अन्तिम दिनों में रानू से क्या मिला ? वह क्या सिर्फ ‘आँसुओं में दुख की शोभा’ बनी रह गई ?
सुनील गंगोपाध्याय की कलम से एक अभिनव और अतुलनीय उपन्यास है !
अपने ग्रहस्थ जीवन ने रवीन्द्रनाथ को कभी मानसिक सुख-शान्ति नहीं मिली थी। अचानक एक दिन लम्बी बीमारी भोगने के बाद कवि की प्रिय बेटी माधुरी लता का देहावसान हो गया। कवि टूट गये। उसी दिन अशान्त चित्त से एक भाड़े की गाड़ी लेकर वे भवानीपुर पहुँचे। नम्बर ढूँढ़ने एक घर के सामने रुककर उन्होंने पुकारा-रानू ! रानू !
अपना नाम सुनते ही तेजी से एक बालिका उतर आयी। कवि अपलक उसे देखते रह गये। यह वे किसे देख रहे थे ? यह परी थी या स्वर्ग की कोई अप्सरा ! उसी दिन अट्ठावन वर्षीय कवि से उस बालिका से विचित्र रिश्ता कायम हो गया। रानू कवि के खेल की संगिनी बन गई। नई रचनाओं की प्रेरणादात्री, उनकी खोई ‘बउठान’
और रानू के लिए कवि हो गये उसके प्रिय भानू दादा !
कवि के चीन-भ्रमण के समय उनकी अनुपस्थिति में रानू की शादी तय हो गई। रानू अब सर राजेन मुखर्जी के पुत्र वीरेन की पत्नी बन गई। दो सन्तानों की माँ।
कवि अब वृद्ध थे। उन्हें जीवन के अन्तिम दिनों में रानू से क्या मिला ? वह क्या सिर्फ ‘आँसुओं में दुख की शोभा’ बनी रह गई ?
सुनील गंगोपाध्याय की कलम से एक अभिनव और अतुलनीय उपन्यास है !
रानू और भानु
प्रिय रवि बाबू !
मैंने आपके ‘गल्प गुच्छ’ की सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, समझ भी गई हूँ। सिर्फ ‘क्षुधित पाषाण’ समझ नहीं पाई। अच्छा, वह बूढ़ा जो ईरानी बाँदी की बात कह रहा था, उस बाँदी की कहानी क्यों नहीं सुनाई ? इसे सुनने की बहुत इच्छा करती है। आप लिखिएगा जरूर।
अच्छा ‘जय-पराजय’ कहानी के अन्त में शेखर के साथ राजकुमारी की शादी हुई थी, ऐसा ही है न ? लेकिन मेरी दीदी कहती है कि शेखर मर गया। आप लिखिएगा की शेखर बच गया और राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। ठीक है न ? अगर शेखर की सचमुच मौत हो गई है तो मुझे बड़ा दुःख होगा।
मुझे आपसे मिलने की खू ऽऽऽऽऽ ब इच्छा करती है। एक बार हमारे यहाँ जरूर आइएगा। आइएगा जरूर, नहीं तो आपसे कुट्टी हो जाएगी। आप अगर यहाँ आएँ तो आपको हमारे शयनकक्ष में सोने दूँगी। अपने खिलौने भी दिखाऊँगी।
मैंने आपके ‘गल्प गुच्छ’ की सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं, समझ भी गई हूँ। सिर्फ ‘क्षुधित पाषाण’ समझ नहीं पाई। अच्छा, वह बूढ़ा जो ईरानी बाँदी की बात कह रहा था, उस बाँदी की कहानी क्यों नहीं सुनाई ? इसे सुनने की बहुत इच्छा करती है। आप लिखिएगा जरूर।
अच्छा ‘जय-पराजय’ कहानी के अन्त में शेखर के साथ राजकुमारी की शादी हुई थी, ऐसा ही है न ? लेकिन मेरी दीदी कहती है कि शेखर मर गया। आप लिखिएगा की शेखर बच गया और राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। ठीक है न ? अगर शेखर की सचमुच मौत हो गई है तो मुझे बड़ा दुःख होगा।
मुझे आपसे मिलने की खू ऽऽऽऽऽ ब इच्छा करती है। एक बार हमारे यहाँ जरूर आइएगा। आइएगा जरूर, नहीं तो आपसे कुट्टी हो जाएगी। आप अगर यहाँ आएँ तो आपको हमारे शयनकक्ष में सोने दूँगी। अपने खिलौने भी दिखाऊँगी।
इति रानू
सुबह की डाक से काफी चिट्ठियाँ और पत्र-पत्रिकाएँ आई थीं। ताजी-ताजी
चिट्ठियाँ पढ़ लेना कवि की आदत बन गई थी। किसी-किसी चिट्ठी का जवाब भी
तुरन्त देने बैठ जाते थे।
इस चिट्ठी को पढ़कर कवि कुछ देर चकित होकर खिड़की की ओर देखते रहे।
तिमंजिले के इस कमरे की खिड़की से आसमान का काफी हिस्सा दिखता था। कुछ सोचते वक्त कवि की आँखें आसमान की ओर चली जाती थीं। चारदीवारी के दायरे से निकलकर मन विस्तीर्ण परिसर में भाग निकलता था, मानो शून्य में काफी रचनाएँ या रेखाचित्र खिल उठे हों।
आज आसमान में सुबह से ही बदली छाई थी।
कल रात-भर सिर्फ गर्मी ही थी ऐसा नहीं हवा भी एकदम बन्द थी। प्रकृति का सब कुछ स्तब्ध था। कवि को गर्मी में जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, गर्मी उन्हें महसूस ही नहीं होती थी। पसीने की बूँदों से पीठ भर जाने पर भी उन्हें कोई असहजता नहीं होती थी।
सावन में ऐसी उमस होते ही यह स्पष्ट था कि बारिश होगी। बादल भी काफी घिर आए थे। कवि को बरसात इतनी प्रिय थी कि वे प्यासे चातक की तरह बार-बार बादल की ओर देखते रहते थे। सब ऋतुओं में उन्हें वर्षा ऋतु ही सर्वाधिक प्रिय थी।
उस चिट्ठी को उन्होंने दो बार पढ़ा। चिट्ठी भेजनेवाली ने अपनी पदवी नहीं, सिर्फ नाम लिखा था। हाँ, पता ज़रूर लिखा था, बनारस का।
यह रानू कौन थी ? कितनी उम्र रही होगी ? चिट्ठी की भाषा से वह कम उम्र की लगती थी, लेकिन सम्बोधन उसने बड़ी गम्भीरता से किया था-प्रिय रवि बाबू ! पहले या बाद में आदर या प्रणाम जताने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी थी। ‘आपको हमारे शयनकक्ष में सोने देंगे’ इस अंश को पढ़कर कवि के चेहरे पर दाढ़ी-मूँछ की आड़ में कौतूहली मुस्कान झलक उठी। क्या यही सबसे ज्यादा खातिरदारी थी ? उन्हें अभी तक किसी के बैठकखाने या बरामदे में सोने का आमन्त्रण नहीं मिला था।
रानू ? कवि की एक बेटी का भी यही नाम था। वह अब इस दुनिया में नहीं थी। सीने में भरा अभिमान लेकर वह इस धरती से चली गई थी।
गड़-गड़ करके बादलों का गरजना शुरू हो गया। जैसे डंके की चोट पर हाथी पर सवार होकर वर्षा आ रही थी। अचानक हवा काफी तेज चलने लगी। कवि बरामदे में आकर खड़े हो गए। पहली बौछार का उन्होंने सिर झुकाकर स्वागत किया।
इसके बाद ही नीचे से बुलावा आया।
चिट्ठियों का जवाब देना फिलहाल टल गया।
शान्तिनिकेतन से एक चिन्ताजनक खबर आई थी। वहाँ के चार छात्र बेहद बीमार हो गए थे। उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था-वह बहुत दुष्ट रोग है। इस महायुद्ध के समय से ही इसकी शुरूआत होने के कारण कवि ने इस बीमारी का नाम युद्ध ज्वर दिया था। जिस तरह युद्ध में काफी सैनिक घायल होते हैं, काफी लोग मर जाते हैं, उसी तरह यह रोग भी काफी लोगों को पस्त कर रहा था, कुछ की जान भी ले चुका था।
शान्तिनिकेतन में दवाएँ और एक अच्छे डॉक्टर को भेजना जरूरी था। इस वक्त वे सिर्फ कवि नहीं थे, वे गुरुदेव थे, शान्तिनिकेतन विद्यालय का सारा भार उन पर था। उनके भरोसे ही अभिभावक अपने बच्चे को वहाँ भेजते थे।
वहाँ के छात्रावास की छत बरसात में टपक रही थी। उसकी मरम्मत ज़रूरी थी। वहाँ के लिए एक कला शिक्षक की नियुक्ति भी ज़रूर हो गई थी। मगर रुपए ?
इसके बाद लगातार कई दिन विभिन्न प्रकार की व्यस्तताओं में बीत गए।
फिर वे खुद भी बीमार पड़ गए।
इस वक्त बुखार होने का मतलब ही घबराहट की बात थी। पहले दिन बुखार के बावजूद वे रामानन्द चट्टोपाध्याय से मिलने चले गए। उनका लड़का मलू शान्तिनिकेतन का छात्र था। शाम के वक्त कालिदास और सुकुमार नया गाना सीखने के लिए आए। अपने बुखार की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं की। गाना गाते समय वे खुद भी इसे भूल गए।
कालिदास इतिहास के विद्वान थे और सुकुमार ‘सन्देश’ पत्रिका में कविता, कहानी, नाटक लिखकर न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी मुग्ध किए हुए थे। ये दोनों ही संगीत के प्रति बड़े उत्साही थे।
सुकुमार जैसे हर वक्त कौतुक से भरे रहते थे। वे दोनों हाथ फैलाकर सिर हिलाकर गाना गाते थे। उनकी तुलना में कालिदास कुछ गम्भीर स्वभाव के होते हुए भी सुकुमार की हर बात में अपनी सहमति जताते रहते थे।
इस चिट्ठी को पढ़कर कवि कुछ देर चकित होकर खिड़की की ओर देखते रहे।
तिमंजिले के इस कमरे की खिड़की से आसमान का काफी हिस्सा दिखता था। कुछ सोचते वक्त कवि की आँखें आसमान की ओर चली जाती थीं। चारदीवारी के दायरे से निकलकर मन विस्तीर्ण परिसर में भाग निकलता था, मानो शून्य में काफी रचनाएँ या रेखाचित्र खिल उठे हों।
आज आसमान में सुबह से ही बदली छाई थी।
कल रात-भर सिर्फ गर्मी ही थी ऐसा नहीं हवा भी एकदम बन्द थी। प्रकृति का सब कुछ स्तब्ध था। कवि को गर्मी में जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, गर्मी उन्हें महसूस ही नहीं होती थी। पसीने की बूँदों से पीठ भर जाने पर भी उन्हें कोई असहजता नहीं होती थी।
सावन में ऐसी उमस होते ही यह स्पष्ट था कि बारिश होगी। बादल भी काफी घिर आए थे। कवि को बरसात इतनी प्रिय थी कि वे प्यासे चातक की तरह बार-बार बादल की ओर देखते रहते थे। सब ऋतुओं में उन्हें वर्षा ऋतु ही सर्वाधिक प्रिय थी।
उस चिट्ठी को उन्होंने दो बार पढ़ा। चिट्ठी भेजनेवाली ने अपनी पदवी नहीं, सिर्फ नाम लिखा था। हाँ, पता ज़रूर लिखा था, बनारस का।
यह रानू कौन थी ? कितनी उम्र रही होगी ? चिट्ठी की भाषा से वह कम उम्र की लगती थी, लेकिन सम्बोधन उसने बड़ी गम्भीरता से किया था-प्रिय रवि बाबू ! पहले या बाद में आदर या प्रणाम जताने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी थी। ‘आपको हमारे शयनकक्ष में सोने देंगे’ इस अंश को पढ़कर कवि के चेहरे पर दाढ़ी-मूँछ की आड़ में कौतूहली मुस्कान झलक उठी। क्या यही सबसे ज्यादा खातिरदारी थी ? उन्हें अभी तक किसी के बैठकखाने या बरामदे में सोने का आमन्त्रण नहीं मिला था।
रानू ? कवि की एक बेटी का भी यही नाम था। वह अब इस दुनिया में नहीं थी। सीने में भरा अभिमान लेकर वह इस धरती से चली गई थी।
गड़-गड़ करके बादलों का गरजना शुरू हो गया। जैसे डंके की चोट पर हाथी पर सवार होकर वर्षा आ रही थी। अचानक हवा काफी तेज चलने लगी। कवि बरामदे में आकर खड़े हो गए। पहली बौछार का उन्होंने सिर झुकाकर स्वागत किया।
इसके बाद ही नीचे से बुलावा आया।
चिट्ठियों का जवाब देना फिलहाल टल गया।
शान्तिनिकेतन से एक चिन्ताजनक खबर आई थी। वहाँ के चार छात्र बेहद बीमार हो गए थे। उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था-वह बहुत दुष्ट रोग है। इस महायुद्ध के समय से ही इसकी शुरूआत होने के कारण कवि ने इस बीमारी का नाम युद्ध ज्वर दिया था। जिस तरह युद्ध में काफी सैनिक घायल होते हैं, काफी लोग मर जाते हैं, उसी तरह यह रोग भी काफी लोगों को पस्त कर रहा था, कुछ की जान भी ले चुका था।
शान्तिनिकेतन में दवाएँ और एक अच्छे डॉक्टर को भेजना जरूरी था। इस वक्त वे सिर्फ कवि नहीं थे, वे गुरुदेव थे, शान्तिनिकेतन विद्यालय का सारा भार उन पर था। उनके भरोसे ही अभिभावक अपने बच्चे को वहाँ भेजते थे।
वहाँ के छात्रावास की छत बरसात में टपक रही थी। उसकी मरम्मत ज़रूरी थी। वहाँ के लिए एक कला शिक्षक की नियुक्ति भी ज़रूर हो गई थी। मगर रुपए ?
इसके बाद लगातार कई दिन विभिन्न प्रकार की व्यस्तताओं में बीत गए।
फिर वे खुद भी बीमार पड़ गए।
इस वक्त बुखार होने का मतलब ही घबराहट की बात थी। पहले दिन बुखार के बावजूद वे रामानन्द चट्टोपाध्याय से मिलने चले गए। उनका लड़का मलू शान्तिनिकेतन का छात्र था। शाम के वक्त कालिदास और सुकुमार नया गाना सीखने के लिए आए। अपने बुखार की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं की। गाना गाते समय वे खुद भी इसे भूल गए।
कालिदास इतिहास के विद्वान थे और सुकुमार ‘सन्देश’ पत्रिका में कविता, कहानी, नाटक लिखकर न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी मुग्ध किए हुए थे। ये दोनों ही संगीत के प्रति बड़े उत्साही थे।
सुकुमार जैसे हर वक्त कौतुक से भरे रहते थे। वे दोनों हाथ फैलाकर सिर हिलाकर गाना गाते थे। उनकी तुलना में कालिदास कुछ गम्भीर स्वभाव के होते हुए भी सुकुमार की हर बात में अपनी सहमति जताते रहते थे।
इसी तरह यदि दिन बीते/तो बीते
मन उड़ता है तो/उड़े गीत के पंखों को फैलाकर
मन उड़ता है तो/उड़े गीत के पंखों को फैलाकर
सुकुमार को यह गीत बहुत प्रिय था। इसका अन्तरा अभी भी उनसे सध नहीं पाया
था-‘अपने हृदय को आज फैलाया धरा ने...’
कालिदास कवि के मुँह से कोई नया गीत सुनना चाहते थे। कवि कॉपी के पन्ने पलटने लगे। उनका रचित गीत कुछ गम्भीर प्रकृति के देशप्रेम से भरा था।
कालिदास कवि के मुँह से कोई नया गीत सुनना चाहते थे। कवि कॉपी के पन्ने पलटने लगे। उनका रचित गीत कुछ गम्भीर प्रकृति के देशप्रेम से भरा था।
तेरी भेरी के मंद्रित स्वर
देश-देश में वंदित करके
घेरा तेरा आसन आकर
वीरों के दल ने
देश-देश में वंदित करके
घेरा तेरा आसन आकर
वीरों के दल ने
गाते-गाते कवि का स्वर एक समय गम्भीर होकर गूँजने लगा-‘दुर्जय
आह्वान है भैरव तुम्हारा, प्रेरित करो...’
उस गीत को सुनते हुए सुकुमार और कालिदास समझ नहीं पाए कि कवि की तबीयत ठीक नहीं है।
अगले दिन प्रतिमा को इसका पता चला। रथी बेहद परेशान हो गया। इस तरह के बुखार की कतई अवहेलना नहीं की जा सकती। उन दिनों विधान रायनाम के एक युवक डॉक्टर काफी चर्चित थे। उन्हें बुलाया गया। घर आकर मरीज़ को देखने की उनकी फीस सोलह रुपए थी तथा गाड़ी-भाड़ा अलग से।
डॉक्टर आकर सम्पूर्ण विश्राम का निर्देश दे गए।
विश्राम मतलब लेटे रहना। मगर लेटे-लेटे भी तो लेखन कार्य किया जा सकता था। संगीत विषयक एक लेख लिखने के लिए प्रथम बार-बार तकादा लगा रहे थे। उस लेख को लिखते समय कवि को याद आया कि उन्होंने अभी तक चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया है।
वे हर चिट्ठी का जवाब देते थे। कोई कष्ट करके पत्र लिखे मगर उसका जवाब न पाए, यह उनकी नजर में पत्र पानेवाले की असभ्यता थी। रानू नाम की लड़की को भी उन्होंने चिट्ठी भेज दी। उसके परिचय और उम्र से वाकिफ न होने के कारण उन्होंने एक औपचारिक चिट्ठी लिख दी।
उनका मन शान्तिनिकेतन की ओर लगा था। बुखार के कारण वे जा नहीं पा रहे थे। वर्षा में शान्तिनिकेतन के सौन्दर्य के क्या कहने !
अपनी बीमारी से ज्यादा चिन्ता उन्हें उन चार छात्रों की बीमारी की थी। वहाँ उन्होंने एक डॉक्टर भेज दिया था। कई दिनों के बाद उन छात्रों की हालत बेहतर होने की खबर पाकर कवि का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा।
शरीर से वे बेहद कमजोर हो गए थे मगर उनका बुखार उतर गया था। कवि को फिर एक बार बरसात में भीगने की इच्छा हुई। उनके मन में एक नए गीत के भाव जगे-
उस गीत को सुनते हुए सुकुमार और कालिदास समझ नहीं पाए कि कवि की तबीयत ठीक नहीं है।
अगले दिन प्रतिमा को इसका पता चला। रथी बेहद परेशान हो गया। इस तरह के बुखार की कतई अवहेलना नहीं की जा सकती। उन दिनों विधान रायनाम के एक युवक डॉक्टर काफी चर्चित थे। उन्हें बुलाया गया। घर आकर मरीज़ को देखने की उनकी फीस सोलह रुपए थी तथा गाड़ी-भाड़ा अलग से।
डॉक्टर आकर सम्पूर्ण विश्राम का निर्देश दे गए।
विश्राम मतलब लेटे रहना। मगर लेटे-लेटे भी तो लेखन कार्य किया जा सकता था। संगीत विषयक एक लेख लिखने के लिए प्रथम बार-बार तकादा लगा रहे थे। उस लेख को लिखते समय कवि को याद आया कि उन्होंने अभी तक चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया है।
वे हर चिट्ठी का जवाब देते थे। कोई कष्ट करके पत्र लिखे मगर उसका जवाब न पाए, यह उनकी नजर में पत्र पानेवाले की असभ्यता थी। रानू नाम की लड़की को भी उन्होंने चिट्ठी भेज दी। उसके परिचय और उम्र से वाकिफ न होने के कारण उन्होंने एक औपचारिक चिट्ठी लिख दी।
उनका मन शान्तिनिकेतन की ओर लगा था। बुखार के कारण वे जा नहीं पा रहे थे। वर्षा में शान्तिनिकेतन के सौन्दर्य के क्या कहने !
अपनी बीमारी से ज्यादा चिन्ता उन्हें उन चार छात्रों की बीमारी की थी। वहाँ उन्होंने एक डॉक्टर भेज दिया था। कई दिनों के बाद उन छात्रों की हालत बेहतर होने की खबर पाकर कवि का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा।
शरीर से वे बेहद कमजोर हो गए थे मगर उनका बुखार उतर गया था। कवि को फिर एक बार बरसात में भीगने की इच्छा हुई। उनके मन में एक नए गीत के भाव जगे-
पथ को भूला
व्याकुल होकर भ्रूमर मर गया
वकुल फूल में
कोई गोपन वाणी करती कानाफूसी
आकाश में वातास से
वन का अंचल भरा पुलक से
लगा झूमने....
व्याकुल होकर भ्रूमर मर गया
वकुल फूल में
कोई गोपन वाणी करती कानाफूसी
आकाश में वातास से
वन का अंचल भरा पुलक से
लगा झूमने....
इस गीत के स्वर को गुनगुनाते हुए उसका संगीत भी नए प्रकार का हो गया।
बीमारी के अलावा भी सुख में बाधा पड़ने के और भी कई कारण होते हैं। कवि राजनीतिक झंझटों की लपेट में आ गए।
सरकार ने नए सिरे से दमन चक्र शुरू कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक से उनकी पत्रिका बन्द करने के लिए कह दिया गया था। ऐनी बेसेंट पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। उनके बम्बई और मध्य प्रदेश में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं ऐनी बेसेंट को भी मद्रास में नज़र बन्द कर दिया गया।
इसके विरोध में पूरा देश मुखर हो उठा। सरकार को उपयुक्त जवाब देने के लिए मद्रास के तेजस्वी पूर्व न्यायधीश सर सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उन्हें अंग्रेज शासकों द्वारा प्रदान की गई सर और दीवान बहादुर की उपाधि लौटा दी और यह प्रस्तावित किया कि उस बार के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ऐनी बेसेंट को ही अध्यक्ष बनाया जाए।
विभिन्न राज्य कांग्रेस कमेटियों ने इस प्रस्ताव का साग्रह अनुमोदन किया मगर बंगाल में आम राय कायम नहीं हो पाई। बांग्ला कांग्रेस में दलबन्दी तो लगी ही रहती थी, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर मतभेद तीव्र हो गया। दो पक्षों के बीच बहस और हल्ले-गुल्ले में सभा की कार्यवाही स्थगित हो गई।
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे कांग्रेस के एक वर्ग के नरमपन्थी नेताओं की धारणा थी कि चूँकि इस विश्वयुद्ध में अंग्रेजों को भारत से काफी सेना और सम्पत्ति लेने के लिए विवश होना पड़ा था, लिहाजा बदले में युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार भारतीयों को स्वायत्त शासन देने के लिए बाध्य होगी। हाल ही में विलायत की पार्लियामेंट में भारत सचिव ने ऐसा आश्वासन दिया भी था। इसलिए इस वक्त सरकार को नाराज न करके उसके साथ सहयोग करना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ चितरंजन दास जैसे चरमपन्थी नेताओं की दृढ़ धारणा थी कि सरकार इतनी आसानी से स्वायत्त शासन देनेवाली नहीं है। भारत सचिव का यह आश्वासन निरा धोखाधड़ी या बहलाने की बात है।
राज्य कांग्रेस के वोटों का विभाजन देखकर चरमपन्थियों ने ठीक किया कि स्वागत समिति के अध्यक्ष के पद पर सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मनोनीत किया जाए। ऐसा होने पर आम सदस्य उनके समर्थन में वोट देंगे। फिर ऐनी बेसेंट को राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कराना आसान हो जाएगा। एक सुबह चितरंजन दास, विपिनचन्द्र पाल, फजलुल हक तथा और भी कई लोग रवीन्द्रनाथ से मिलने पहुँचे।
रवीन्द्रनाथ ऐनी बेसेंट का आदर करते थे। अंग्रेज सरकार के कुशासन के विरुद्ध वे गरिमामयी अंग्रेज महिला आम जनता को जागृत करने के लिए अनथक परिश्रम कर रही थीं। उनका समर्थन करना एकदम उचित था। उन्हें नजरबन्द करके सरकार उनको अपमानित करना चाहती थी, इसलिए भारतवासियों का कर्त्तव्य था कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन किया जाए।
लेकिन रवीन्द्रनाथ ने कभी भी सीधे-सीधे अपने को राजनीति से नहीं जोड़ा था। बस, लगभग एक युग पहले, बंग-भंग के प्रस्ताव के समय उन्होंने सड़क पर उतरकर जुलूस में भाग लिया था। मगर वह पूरी तौर से राजनीति नहीं थी, वह भावना का सम्बन्ध था। इसके बाद राजनीतिक नेताओं के द्वारा उसका मोर्चा सँभाल लिये जाने के बाद उन्होंने इस आन्दोलन से किनारा कर लिया था। किसी कवि के लिए राजनीति से दूर रहना ही उचित होता है।
लेकिन ऐसे संकट के समय, उनके नाम के इस्तेमाल से अलग एक महान काम सम्पन्न हो सकता हो तब क्या उससे विमुख हुआ जा सकता है ? अपने कई मित्रों के निषेध के बावजूद वे इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। इसकी खबर सभी समाचार पत्रों में छप गई।
बीमारी के अलावा भी सुख में बाधा पड़ने के और भी कई कारण होते हैं। कवि राजनीतिक झंझटों की लपेट में आ गए।
सरकार ने नए सिरे से दमन चक्र शुरू कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक से उनकी पत्रिका बन्द करने के लिए कह दिया गया था। ऐनी बेसेंट पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। उनके बम्बई और मध्य प्रदेश में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं ऐनी बेसेंट को भी मद्रास में नज़र बन्द कर दिया गया।
इसके विरोध में पूरा देश मुखर हो उठा। सरकार को उपयुक्त जवाब देने के लिए मद्रास के तेजस्वी पूर्व न्यायधीश सर सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उन्हें अंग्रेज शासकों द्वारा प्रदान की गई सर और दीवान बहादुर की उपाधि लौटा दी और यह प्रस्तावित किया कि उस बार के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ऐनी बेसेंट को ही अध्यक्ष बनाया जाए।
विभिन्न राज्य कांग्रेस कमेटियों ने इस प्रस्ताव का साग्रह अनुमोदन किया मगर बंगाल में आम राय कायम नहीं हो पाई। बांग्ला कांग्रेस में दलबन्दी तो लगी ही रहती थी, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर मतभेद तीव्र हो गया। दो पक्षों के बीच बहस और हल्ले-गुल्ले में सभा की कार्यवाही स्थगित हो गई।
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे कांग्रेस के एक वर्ग के नरमपन्थी नेताओं की धारणा थी कि चूँकि इस विश्वयुद्ध में अंग्रेजों को भारत से काफी सेना और सम्पत्ति लेने के लिए विवश होना पड़ा था, लिहाजा बदले में युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार भारतीयों को स्वायत्त शासन देने के लिए बाध्य होगी। हाल ही में विलायत की पार्लियामेंट में भारत सचिव ने ऐसा आश्वासन दिया भी था। इसलिए इस वक्त सरकार को नाराज न करके उसके साथ सहयोग करना ही बेहतर होगा। दूसरी तरफ चितरंजन दास जैसे चरमपन्थी नेताओं की दृढ़ धारणा थी कि सरकार इतनी आसानी से स्वायत्त शासन देनेवाली नहीं है। भारत सचिव का यह आश्वासन निरा धोखाधड़ी या बहलाने की बात है।
राज्य कांग्रेस के वोटों का विभाजन देखकर चरमपन्थियों ने ठीक किया कि स्वागत समिति के अध्यक्ष के पद पर सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मनोनीत किया जाए। ऐसा होने पर आम सदस्य उनके समर्थन में वोट देंगे। फिर ऐनी बेसेंट को राष्ट्रीय अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कराना आसान हो जाएगा। एक सुबह चितरंजन दास, विपिनचन्द्र पाल, फजलुल हक तथा और भी कई लोग रवीन्द्रनाथ से मिलने पहुँचे।
रवीन्द्रनाथ ऐनी बेसेंट का आदर करते थे। अंग्रेज सरकार के कुशासन के विरुद्ध वे गरिमामयी अंग्रेज महिला आम जनता को जागृत करने के लिए अनथक परिश्रम कर रही थीं। उनका समर्थन करना एकदम उचित था। उन्हें नजरबन्द करके सरकार उनको अपमानित करना चाहती थी, इसलिए भारतवासियों का कर्त्तव्य था कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन किया जाए।
लेकिन रवीन्द्रनाथ ने कभी भी सीधे-सीधे अपने को राजनीति से नहीं जोड़ा था। बस, लगभग एक युग पहले, बंग-भंग के प्रस्ताव के समय उन्होंने सड़क पर उतरकर जुलूस में भाग लिया था। मगर वह पूरी तौर से राजनीति नहीं थी, वह भावना का सम्बन्ध था। इसके बाद राजनीतिक नेताओं के द्वारा उसका मोर्चा सँभाल लिये जाने के बाद उन्होंने इस आन्दोलन से किनारा कर लिया था। किसी कवि के लिए राजनीति से दूर रहना ही उचित होता है।
लेकिन ऐसे संकट के समय, उनके नाम के इस्तेमाल से अलग एक महान काम सम्पन्न हो सकता हो तब क्या उससे विमुख हुआ जा सकता है ? अपने कई मित्रों के निषेध के बावजूद वे इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। इसकी खबर सभी समाचार पत्रों में छप गई।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book